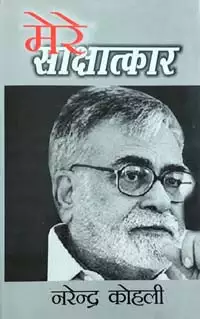|
हास्य-व्यंग्य >> पाँच एब्सर्ड उपन्यास पाँच एब्सर्ड उपन्यासनरेन्द्र कोहली
|
123 पाठक हैं |
|||||||
हास्य-व्यंग्य पर आधारित मनोरंजक पुस्तक....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
जब एक उपन्यासकार की कलम, कार्टूनिस्ट की दृष्टि पा जाती है तो एब्सर्ड
उपन्यासों की रचना होती है। नरेन्द्र कोहली की इन पाँच रचनाओं में आपको
उपन्यास का गठन, व्यंग्य-चित्रकार की पैनी दृष्टि, एक अनोखा अप्रस्तुत
विधान, तीखा-करारा व्यंग्य तथा समकालीन जीवन की कुतर्कशीलता अपनी समग्रता
में उपलब्ध होगी।
सर्वथा नवीन कथ्य, शिल्प, शैली और विधा !
व्यंग्य लेखन का एक सर्वथा नवीन आयाम !
इन रचनाओं में आपको व्यंग्य अपनी संपूर्ण गम्भीरता में मिलेगा और आप समझ पाएँगे कि व्यंग्य हसाने के साथ-साथ रुला भी सकता है, घावों को कुरेद भी सकता है और व्यक्ति को उसके आक्रोश का जीवन्त साक्षात्कार भी करा सकता है।
सर्वथा नवीन कथ्य, शिल्प, शैली और विधा !
व्यंग्य लेखन का एक सर्वथा नवीन आयाम !
इन रचनाओं में आपको व्यंग्य अपनी संपूर्ण गम्भीरता में मिलेगा और आप समझ पाएँगे कि व्यंग्य हसाने के साथ-साथ रुला भी सकता है, घावों को कुरेद भी सकता है और व्यक्ति को उसके आक्रोश का जीवन्त साक्षात्कार भी करा सकता है।
तेईस वर्ष बाद
‘पाँच एब्सर्ड उपन्यास’ का पहला संस्करण दिसंबर 1971
में तैयार हो गया था। उसके पश्चात् दो-एक संस्करण और भी हुए। इधर वर्षों
से यह पुस्तक अप्राप्य थी। मुझे प्रसन्नता है कि प्रायः तेईस वर्षों के
पश्चात् यह अपने नए रूप में, प्रकाशित होकर, पाठको के सम्मुख आ रही है।
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने एक पत्र में मुझे ‘एब्सर्ड’ शब्द के पर्याय के रूप में ‘अवश्रद्ध’ शब्द सुझाया था, जो ध्वनि और अर्थ, दोनों ही दृष्टियों से ‘एब्सर्ड’ के बहुत निकट का शब्द है...और फिर हमारा अपना शब्द है। यह शब्द मुझे बहुत भाया। इच्छा हुई कि पुस्तक का शीर्षक बदल दूँ।...किंतु प्रचलन का अपना बल होता है। जो नाम प्रचलित हो गया, वह हो गया। पुस्तक फिर पुराने नाम से ही जा रही है; किंतु द्विवेदी जी का स्मरण किए बिना नहीं रहा जाता।
इन तेईस वर्षों में व्यंग्य ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है। मुझसे वरिष्ठ तथा मेरे समकालीन व्यंग्यकारों की अनेक नई रचनाएँ तो आई ही हैं; अनेक नए व्यंग्यकारों ने भी हिंदी-व्यंग्य को समृद्ध किया है। मुझे प्रसन्नता है कि हिंदी में व्यंग्यकारों के नामों की संख्या, तीन या चार तक ही सीमित नहीं रह गई है। राधाकृष्ण, परसाई, शरद जोशी, रवीन्द्रनाथ त्यागी तथा श्रीलाल शुक्ल के साथ अब लक्ष्मीकांत वैष्णव, प्रेम जनमेजय, सुरेश कांत, ज्ञान चतुर्वेदी, अंजनी चौहान, राजेश कुमार, सूर्यबाला, कृष्ण चराटे, लतीफ घोंघी, शंकर पुणतांबेकर, सुदर्शन मजीठिया, ईश्वर शर्मा, हरि जोशी, मनोहर श्याम जोशी, सुभाष अखिल सी. भास्कर राव, नरेन्द्र मौर्य, गोपाल चतुर्वेदी, प्रदीप पंत, के .पी. सक्सेना, अजातशत्रु, अवतार सिंह, श्रीराम आयंगार, दामोदर दत्त दीक्षित, मधुसूदन पाटिल, विनोद शंकर शुक्ल, राजेन्द्र राव, महेशचंद्र, महेश दत्त शर्मा, विजय त्रिपाठी, नवीनचंद्र लोनी, सत्यप्रकाश अग्रवाल ‘उमंग’, विनोद साव, महेन्द्र वाशिष्ठ, धनराज चौधरी, अश्विनी कुमार दुबे, स्नेहलता पाठक, त्रिभुवन पांडेय, शिवानक कामड़े, कस्तूरी दिनेश, प्रकाश पुरोहित, विजय कृष्ण ठाकुर, हरीश नवल...कितने ही नाम जुड़ गए हैं, और लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। यह कोई प्रामाणिक सूची नहीं है, केवल इस बात का संकेत है कि व्यंग्य, असंख्य युवा लेखकों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है, ताकि वे अंधकार और भ्रष्टाचार से लड़ें और प्रकाश की खोज में आगे बढ़ें। अब आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी के समर्थ आलोचक और साहित्य-मर्मज्ञ इन नई प्रतिभाओं को पहचानें और उनका उचित सम्मान करें। इस प्रकार के आलोचक कर्म के लिए मैं डॉ. बालेन्दु शेखर तिवारी तथा श्याम सुंदर घोष के प्रयत्नों का पर्याप्त प्रशंसक हूँ।
अनेक लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं उपन्यासों के साथ-साथ व्यंग्य-लेखन तो आज तक कर रहा हूँ; किंतु मैंने पाँचवे के बाद छटा एब्सर्ड क्यों नहीं लिखा ?...जिज्ञासा उचित ही है। किंतु क्या करता : रचना तो अपना शिल्प स्वयं ढूँढ़ती है, जैसे आत्मा अपनी इच्छानुसार शरीर का वरण करती है। पुनरावृत्ति के लिए पुनरावृत्ति, मौलिकता को नष्ट करती है। मैं लेखक द्वारा अपने शिल्प का अनुकरण भी उचित नहीं समझता। इसलिए ‘पाँच एब्सर्ड उपन्यास’, ‘आश्रितों का विद्रोह’ ‘शंबूक की हत्या’ तथा अन्य संकलनों में सामग्री के अनुसार ही शिल्प चुना गया है।
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने एक पत्र में मुझे ‘एब्सर्ड’ शब्द के पर्याय के रूप में ‘अवश्रद्ध’ शब्द सुझाया था, जो ध्वनि और अर्थ, दोनों ही दृष्टियों से ‘एब्सर्ड’ के बहुत निकट का शब्द है...और फिर हमारा अपना शब्द है। यह शब्द मुझे बहुत भाया। इच्छा हुई कि पुस्तक का शीर्षक बदल दूँ।...किंतु प्रचलन का अपना बल होता है। जो नाम प्रचलित हो गया, वह हो गया। पुस्तक फिर पुराने नाम से ही जा रही है; किंतु द्विवेदी जी का स्मरण किए बिना नहीं रहा जाता।
इन तेईस वर्षों में व्यंग्य ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है। मुझसे वरिष्ठ तथा मेरे समकालीन व्यंग्यकारों की अनेक नई रचनाएँ तो आई ही हैं; अनेक नए व्यंग्यकारों ने भी हिंदी-व्यंग्य को समृद्ध किया है। मुझे प्रसन्नता है कि हिंदी में व्यंग्यकारों के नामों की संख्या, तीन या चार तक ही सीमित नहीं रह गई है। राधाकृष्ण, परसाई, शरद जोशी, रवीन्द्रनाथ त्यागी तथा श्रीलाल शुक्ल के साथ अब लक्ष्मीकांत वैष्णव, प्रेम जनमेजय, सुरेश कांत, ज्ञान चतुर्वेदी, अंजनी चौहान, राजेश कुमार, सूर्यबाला, कृष्ण चराटे, लतीफ घोंघी, शंकर पुणतांबेकर, सुदर्शन मजीठिया, ईश्वर शर्मा, हरि जोशी, मनोहर श्याम जोशी, सुभाष अखिल सी. भास्कर राव, नरेन्द्र मौर्य, गोपाल चतुर्वेदी, प्रदीप पंत, के .पी. सक्सेना, अजातशत्रु, अवतार सिंह, श्रीराम आयंगार, दामोदर दत्त दीक्षित, मधुसूदन पाटिल, विनोद शंकर शुक्ल, राजेन्द्र राव, महेशचंद्र, महेश दत्त शर्मा, विजय त्रिपाठी, नवीनचंद्र लोनी, सत्यप्रकाश अग्रवाल ‘उमंग’, विनोद साव, महेन्द्र वाशिष्ठ, धनराज चौधरी, अश्विनी कुमार दुबे, स्नेहलता पाठक, त्रिभुवन पांडेय, शिवानक कामड़े, कस्तूरी दिनेश, प्रकाश पुरोहित, विजय कृष्ण ठाकुर, हरीश नवल...कितने ही नाम जुड़ गए हैं, और लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। यह कोई प्रामाणिक सूची नहीं है, केवल इस बात का संकेत है कि व्यंग्य, असंख्य युवा लेखकों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है, ताकि वे अंधकार और भ्रष्टाचार से लड़ें और प्रकाश की खोज में आगे बढ़ें। अब आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी के समर्थ आलोचक और साहित्य-मर्मज्ञ इन नई प्रतिभाओं को पहचानें और उनका उचित सम्मान करें। इस प्रकार के आलोचक कर्म के लिए मैं डॉ. बालेन्दु शेखर तिवारी तथा श्याम सुंदर घोष के प्रयत्नों का पर्याप्त प्रशंसक हूँ।
अनेक लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं उपन्यासों के साथ-साथ व्यंग्य-लेखन तो आज तक कर रहा हूँ; किंतु मैंने पाँचवे के बाद छटा एब्सर्ड क्यों नहीं लिखा ?...जिज्ञासा उचित ही है। किंतु क्या करता : रचना तो अपना शिल्प स्वयं ढूँढ़ती है, जैसे आत्मा अपनी इच्छानुसार शरीर का वरण करती है। पुनरावृत्ति के लिए पुनरावृत्ति, मौलिकता को नष्ट करती है। मैं लेखक द्वारा अपने शिल्प का अनुकरण भी उचित नहीं समझता। इसलिए ‘पाँच एब्सर्ड उपन्यास’, ‘आश्रितों का विद्रोह’ ‘शंबूक की हत्या’ तथा अन्य संकलनों में सामग्री के अनुसार ही शिल्प चुना गया है।
नरेन्द्र कोहली
आत्मकथ्य
‘अस्पताल’ की रचना बड़ी ही पीड़ि़त मनःस्थिति में हुई
है : अब सोचता हूँ तो लगता है कि जब तक सह सकता था सहा, पर जब सह न सका तो
मैं व्यंग्य करने पर उतर आया। पीड़ा ने ही मुझे अपने से कुछ बड़ा कर दिया
था और ऐसी आँख दी थी जिसने उस सारे वातावरण को एक कार्टून की दृष्टि से
देखा था। और यह सब शायद इसीलिए हुआ था ताकि मैं अपना मानसिक सन्तुलन स्थिर
रखकर जी सकूँ...
24 दिसंबर, 1967 की कड़ा़केदार सर्दियों की रात में दिल्ली के ‘आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़’ के चिल्ड्रन-वार्ड के एक कमरे में मैं और मेरी पत्नी दो मेज़ों के बीच बैठे हुए थे। एक मेज़ की ओर हमारे चेहरे थे। हमारी आँखें उस पर टिकी हुई थीं, और हमारे प्राण हमारी आँखों में समाए हुए थे। उस मेज़ पर हमारे जुड़वाँ बच्चों में से एक—कार्तिकेय, मृत्यु के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। वह बुरी तरह डायरिया से पीड़ित था और उसके शरीर का सारा पानी प्रायः निकल चुका था। चौबीस दिन के नन्हें बच्चे के शरीर के अंग-अंग को सुइयों से भेदा जा चुका था और शिरा (Vein) न मिलने के कारण उसकी नाक में नली लगाकर ग्लूकोस उसके शरीर में पहुँचाया जा रहा था। और हम—पति-पत्नी—अपनी आँखों के माध्यम से उसके शरीर का एक-एक स्पंदन चुग रहे थे, उसकी एक-एक साँस गिन रहे थे...
हमारी पिछली मेज़ पर (जिसकी ओर पीठ किए हम दोनों ही उसे भूलने की कोशिश कर रह थे।) कार्तिकेय की जु़ड़वाँ बहन—जिसे मैंने मरणोपरांत ‘सुरभि’ नाम दिया था—मृत पड़ी थी। उसकी मृत्यु अभी-अभी डिहाइड्रेशन से हो गई थी। डॉक्टरों को उसकी शिरा (Vein) नहीं मिली थी और उसकी खोज में उन्होंने चौबीस दिनों की उस बच्ची के दुर्बल शरीर को जगह-जगह से चीर दिया था, जिन पर अब पट्टियाँ बँधी हुई थीं।
हम दोनों में से कोई रो नहीं रहा था। रोने का अवकाश नहीं था—हमें अपने जीवित बच्चे के प्राणों की चिंता थी।
ऐसे समय में अस्पताल के अधिकारियों की ओर से यह कहा गया था कि मैं बच्चे के पास केवल उसकी माँ को रहने दूँ और स्वयं बाहर चला आऊँ। मुझे लगा था कि यही उचित है। पर माँ को मैं उसके जीवित बच्चे के साथ तो अकेली छोड़ सकता था, मृत बच्चे के साथ नहीं। मैंने बड़े़ विनीत—लगभग रोते हुए—स्वर में उस अधिकारी से कहा था कि मैं चाहता हूँ, मृत बच्ची के शरीर को वहाँ से हटा लिया जाए ताकि माँ को जीवित बच्चे के साथ अकेली छोड़ा जा सके। पर इतनी सर्दी में रात के इस समय मैं बच्ची के शरीर को अंतिम क्रिया के लिए नहीं ले जा सकूँगा। फिर, जीवित बच्चा अभी मृत्यु के पंजे में पड़ा है, अतः उसे छोड़कर मृत बच्ची की ओर ध्यान देने का मुझे अवकाश नहीं है। क्या वे लोग कृपा करके मृत बच्ची के शरीर को सुबह तक शवशाला (मार्चरी) में रख लेंगे ?
तब मुझे एक नर्स ने कहा था, ‘‘हम इसे मार्चरी में रख लेंगे। आप चिंता न करें, मार्चरी एयर-कंडीशंड है और उसमें आप बच्ची को एक हफ्ते के लिए भी छोड़ देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। वह आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी।’’
मैं समझ नहीं सका कि वह स्नेहमयी, वात्सल्य की भंडार और सहानुभूति की मूर्ति नर्स मेरी मृत बच्ची की बात कर रही थी या कोई गृहिणी किन्हीं सब्जियों को फ्रिज में रखने की बात कह रही थी...
और फिर एक के बाद एक ऐसे ही झकझोरने वाले अनुभव। मैं रोता भी था और हँसता भी था। उस मनः स्थिति में कोई मुझसे बच्चे का हाल पूछता तो मैं कहता—‘‘दो बच्चे थे। एक लड़का, एक लड़की ! लड़की 24 दिसंबर को मर गई। लड़का शायद आज चल बसे।’’
लड़के की हालत कुछ सुधरी तो उसे हम घर ले आए। अस्पताल से निकलकर मुझे उसके विषय में सोचने का अवकाश मिला। अस्पताल के वे विभिन्न दृश्य पिशाचों के समान मुझे नोचने लगे। मेरी नसें चटखने लगीं और मेरा सिर भन्नाने लगा। तब मैंने उन पिशाचों से मुक्ति पाने के लिए ‘अस्पताल’ की रचना की थी....
ऊपर की ये पंक्तियां एक पत्रिका के लिए मैंने आत्मकथ्य के रूप में लिखी थीं, जो पत्रिका के प्रकाशन के स्थगित हो जाने के कारण प्रकाशित न हो सकीं। आज सोचता हूँ तो लगता है, एक ‘अस्पताल’ ही क्या, ये पाँचों रचनाएँ उसी पीड़ि़त मनः स्थिति में लिखी गई थीं। संदर्भ चाहे अलग थे, किंतु परिस्थितियों की एब्सर्डिटी सब जगह समान थी, अतः उन्हें एक ही विधा में अभिव्यक्त होना पड़ा। यही कारण है कि यदि इन पाँचों रचनाओं के विषय में ‘आत्मकथ्य’ लिखने बैठूँगा, तो शायद ‘अस्पताल’ के विषय में लिखी हुई बातों को ही बार-बार दोहराऊँगा...
इन पाँचों एब्सर्ड उपन्यासों में से ‘अस्पताल’ तथा ‘दि लाइफ’ ‘धर्मयुग’ में, ‘मुहल्ला’ ‘नई कहानियाँ’ में तथा ‘दि कॉलेज’ (संपादक द्वारा) काफी संशोधित रूप में ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’ में प्रकाशित हुए थे। ‘शफा देने वाले’ अभी तक अप्रकाशित ही है। जब ये रचनाएँ ‘एब्सर्ड उपन्यास’ विधा के नाम से प्रकाशित हुई थीं, तो कुछ लोगों ने मुझसे यह जानना चाहा था कि आखिर अपनी इन रचनाओं को मैंने ‘एब्सर्ड उपन्यास’ का नाम क्यों दिया है ? या एब्सर्ड उपन्यास क्या होता है ?
पर इन जिज्ञासुओं के साथ-साथ मेरे कुछ ऐसे बंधु भी थे, जिन्होंने पाश्चात्य साहित्य (आवश्यकता से अधिक) पढ़ रखा था। उन बंधुओं ने मुझसे कुछ पूछने के स्थान पर मुझे बताया कि पश्चिम में ‘एब्सर्ड’ शब्द एक विशिष्ट, पारिभाषिक शब्द है और उसके पीछे एक विशिष्ट दर्शन है। उन्होंने जो दूसरी सूचना मुझे दी, वह यह है कि ‘हिन्दी वाले’ जानते-समझते तो कुछ हैं नहीं, उठाकर नाम रख देते हैं।
मैंने उनकी सूचना तथा हिन्दीवालों संबंधी धारणा को चुपचाप स्वीकर कर लिया है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि पश्चिम के ‘एब्सर्ड दर्शन से मेरी इन रचनाओं को कुछ लेना-देना नहीं है। यदि पश्चिम के लोग नए दर्शन, नई धाराओं, नई विधाओं का सृजन करने के लिए स्वतंत्र हैं तो हमारे लिए भी यह आवश्यक नहीं है कि हम उनका साहित्य पढ़कर ही अपनी विधाओं का निर्माण करें। पश्चिम का या कहीं का भी साहित्य पढ़ना अच्छी बात है, प्रत्येक जागरुक साहित्यकार विश्वभर के साहित्य से अपना परिचय बढ़ाना चाहता है, किंतु अपने जीवन को अपने साहित्य में चिचित्र करने के लिए पश्चिमी साहित्य की अनुमति लेना मैं अनिवार्य नहीं समझता।
इन एब्सर्ड उपन्यासों में जो जीवन चित्रित है वह हमारा, आपका, हमारे आसपास का जीवन है। वह हमारा जाना-पहचाना अवश्य है, किन्तु अपनी तर्कहीनता के कारण अपनी किसी परिचित विधा में उसका चित्रण मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि कथ्य को उसके अनुरूप शिल्प न मिले तो कथ्य भी पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं हो पाता। यही कारण है कि परिचित तमाम विधाओं को छोड़कर मुझे इस नई विधा का निर्माण करना पड़ा है। अपने कथ्य के अनुरूप मुझे यही शिल्प, यही विधा मिल सकी—अतः मैंने यह देखने का प्रयत्न नहीं किया कि पश्चिम वालों ने इस विधा का प्रयोग पहले किया है या नहीं।
विस्तार में ये रचनाएँ कहानी से अधिक लंबी नहीं हैं—किंतु गठन में, चित्रण की समग्रता के कारण वे उपन्यास हैं। मैं उन्हें उपन्यास ही मानता हूँ, और यही माने जाने का आग्रह करता हूँ। किंतु ये परंपरागत उपन्यास नहीं हैं—अपने अध्यायों के आकार तथा शिल्प एवं शैली के कारण वे परंपरागत उपन्यास नहीं बन पाए। उनके कथ्य की एब्सर्डिटी को उभारने के लिए एब्सर्ड अप्रस्तुत विधान का सहारा लिया गया है। अतः मैंने उन्हें एब्सर्ड उपन्यास का नाम दिया है। आशा है, यह नाम स्वीकार्य होगा।
1-12-1971
24 दिसंबर, 1967 की कड़ा़केदार सर्दियों की रात में दिल्ली के ‘आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़’ के चिल्ड्रन-वार्ड के एक कमरे में मैं और मेरी पत्नी दो मेज़ों के बीच बैठे हुए थे। एक मेज़ की ओर हमारे चेहरे थे। हमारी आँखें उस पर टिकी हुई थीं, और हमारे प्राण हमारी आँखों में समाए हुए थे। उस मेज़ पर हमारे जुड़वाँ बच्चों में से एक—कार्तिकेय, मृत्यु के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। वह बुरी तरह डायरिया से पीड़ित था और उसके शरीर का सारा पानी प्रायः निकल चुका था। चौबीस दिन के नन्हें बच्चे के शरीर के अंग-अंग को सुइयों से भेदा जा चुका था और शिरा (Vein) न मिलने के कारण उसकी नाक में नली लगाकर ग्लूकोस उसके शरीर में पहुँचाया जा रहा था। और हम—पति-पत्नी—अपनी आँखों के माध्यम से उसके शरीर का एक-एक स्पंदन चुग रहे थे, उसकी एक-एक साँस गिन रहे थे...
हमारी पिछली मेज़ पर (जिसकी ओर पीठ किए हम दोनों ही उसे भूलने की कोशिश कर रह थे।) कार्तिकेय की जु़ड़वाँ बहन—जिसे मैंने मरणोपरांत ‘सुरभि’ नाम दिया था—मृत पड़ी थी। उसकी मृत्यु अभी-अभी डिहाइड्रेशन से हो गई थी। डॉक्टरों को उसकी शिरा (Vein) नहीं मिली थी और उसकी खोज में उन्होंने चौबीस दिनों की उस बच्ची के दुर्बल शरीर को जगह-जगह से चीर दिया था, जिन पर अब पट्टियाँ बँधी हुई थीं।
हम दोनों में से कोई रो नहीं रहा था। रोने का अवकाश नहीं था—हमें अपने जीवित बच्चे के प्राणों की चिंता थी।
ऐसे समय में अस्पताल के अधिकारियों की ओर से यह कहा गया था कि मैं बच्चे के पास केवल उसकी माँ को रहने दूँ और स्वयं बाहर चला आऊँ। मुझे लगा था कि यही उचित है। पर माँ को मैं उसके जीवित बच्चे के साथ तो अकेली छोड़ सकता था, मृत बच्चे के साथ नहीं। मैंने बड़े़ विनीत—लगभग रोते हुए—स्वर में उस अधिकारी से कहा था कि मैं चाहता हूँ, मृत बच्ची के शरीर को वहाँ से हटा लिया जाए ताकि माँ को जीवित बच्चे के साथ अकेली छोड़ा जा सके। पर इतनी सर्दी में रात के इस समय मैं बच्ची के शरीर को अंतिम क्रिया के लिए नहीं ले जा सकूँगा। फिर, जीवित बच्चा अभी मृत्यु के पंजे में पड़ा है, अतः उसे छोड़कर मृत बच्ची की ओर ध्यान देने का मुझे अवकाश नहीं है। क्या वे लोग कृपा करके मृत बच्ची के शरीर को सुबह तक शवशाला (मार्चरी) में रख लेंगे ?
तब मुझे एक नर्स ने कहा था, ‘‘हम इसे मार्चरी में रख लेंगे। आप चिंता न करें, मार्चरी एयर-कंडीशंड है और उसमें आप बच्ची को एक हफ्ते के लिए भी छोड़ देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। वह आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी।’’
मैं समझ नहीं सका कि वह स्नेहमयी, वात्सल्य की भंडार और सहानुभूति की मूर्ति नर्स मेरी मृत बच्ची की बात कर रही थी या कोई गृहिणी किन्हीं सब्जियों को फ्रिज में रखने की बात कह रही थी...
और फिर एक के बाद एक ऐसे ही झकझोरने वाले अनुभव। मैं रोता भी था और हँसता भी था। उस मनः स्थिति में कोई मुझसे बच्चे का हाल पूछता तो मैं कहता—‘‘दो बच्चे थे। एक लड़का, एक लड़की ! लड़की 24 दिसंबर को मर गई। लड़का शायद आज चल बसे।’’
लड़के की हालत कुछ सुधरी तो उसे हम घर ले आए। अस्पताल से निकलकर मुझे उसके विषय में सोचने का अवकाश मिला। अस्पताल के वे विभिन्न दृश्य पिशाचों के समान मुझे नोचने लगे। मेरी नसें चटखने लगीं और मेरा सिर भन्नाने लगा। तब मैंने उन पिशाचों से मुक्ति पाने के लिए ‘अस्पताल’ की रचना की थी....
ऊपर की ये पंक्तियां एक पत्रिका के लिए मैंने आत्मकथ्य के रूप में लिखी थीं, जो पत्रिका के प्रकाशन के स्थगित हो जाने के कारण प्रकाशित न हो सकीं। आज सोचता हूँ तो लगता है, एक ‘अस्पताल’ ही क्या, ये पाँचों रचनाएँ उसी पीड़ि़त मनः स्थिति में लिखी गई थीं। संदर्भ चाहे अलग थे, किंतु परिस्थितियों की एब्सर्डिटी सब जगह समान थी, अतः उन्हें एक ही विधा में अभिव्यक्त होना पड़ा। यही कारण है कि यदि इन पाँचों रचनाओं के विषय में ‘आत्मकथ्य’ लिखने बैठूँगा, तो शायद ‘अस्पताल’ के विषय में लिखी हुई बातों को ही बार-बार दोहराऊँगा...
इन पाँचों एब्सर्ड उपन्यासों में से ‘अस्पताल’ तथा ‘दि लाइफ’ ‘धर्मयुग’ में, ‘मुहल्ला’ ‘नई कहानियाँ’ में तथा ‘दि कॉलेज’ (संपादक द्वारा) काफी संशोधित रूप में ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’ में प्रकाशित हुए थे। ‘शफा देने वाले’ अभी तक अप्रकाशित ही है। जब ये रचनाएँ ‘एब्सर्ड उपन्यास’ विधा के नाम से प्रकाशित हुई थीं, तो कुछ लोगों ने मुझसे यह जानना चाहा था कि आखिर अपनी इन रचनाओं को मैंने ‘एब्सर्ड उपन्यास’ का नाम क्यों दिया है ? या एब्सर्ड उपन्यास क्या होता है ?
पर इन जिज्ञासुओं के साथ-साथ मेरे कुछ ऐसे बंधु भी थे, जिन्होंने पाश्चात्य साहित्य (आवश्यकता से अधिक) पढ़ रखा था। उन बंधुओं ने मुझसे कुछ पूछने के स्थान पर मुझे बताया कि पश्चिम में ‘एब्सर्ड’ शब्द एक विशिष्ट, पारिभाषिक शब्द है और उसके पीछे एक विशिष्ट दर्शन है। उन्होंने जो दूसरी सूचना मुझे दी, वह यह है कि ‘हिन्दी वाले’ जानते-समझते तो कुछ हैं नहीं, उठाकर नाम रख देते हैं।
मैंने उनकी सूचना तथा हिन्दीवालों संबंधी धारणा को चुपचाप स्वीकर कर लिया है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि पश्चिम के ‘एब्सर्ड दर्शन से मेरी इन रचनाओं को कुछ लेना-देना नहीं है। यदि पश्चिम के लोग नए दर्शन, नई धाराओं, नई विधाओं का सृजन करने के लिए स्वतंत्र हैं तो हमारे लिए भी यह आवश्यक नहीं है कि हम उनका साहित्य पढ़कर ही अपनी विधाओं का निर्माण करें। पश्चिम का या कहीं का भी साहित्य पढ़ना अच्छी बात है, प्रत्येक जागरुक साहित्यकार विश्वभर के साहित्य से अपना परिचय बढ़ाना चाहता है, किंतु अपने जीवन को अपने साहित्य में चिचित्र करने के लिए पश्चिमी साहित्य की अनुमति लेना मैं अनिवार्य नहीं समझता।
इन एब्सर्ड उपन्यासों में जो जीवन चित्रित है वह हमारा, आपका, हमारे आसपास का जीवन है। वह हमारा जाना-पहचाना अवश्य है, किन्तु अपनी तर्कहीनता के कारण अपनी किसी परिचित विधा में उसका चित्रण मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि कथ्य को उसके अनुरूप शिल्प न मिले तो कथ्य भी पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं हो पाता। यही कारण है कि परिचित तमाम विधाओं को छोड़कर मुझे इस नई विधा का निर्माण करना पड़ा है। अपने कथ्य के अनुरूप मुझे यही शिल्प, यही विधा मिल सकी—अतः मैंने यह देखने का प्रयत्न नहीं किया कि पश्चिम वालों ने इस विधा का प्रयोग पहले किया है या नहीं।
विस्तार में ये रचनाएँ कहानी से अधिक लंबी नहीं हैं—किंतु गठन में, चित्रण की समग्रता के कारण वे उपन्यास हैं। मैं उन्हें उपन्यास ही मानता हूँ, और यही माने जाने का आग्रह करता हूँ। किंतु ये परंपरागत उपन्यास नहीं हैं—अपने अध्यायों के आकार तथा शिल्प एवं शैली के कारण वे परंपरागत उपन्यास नहीं बन पाए। उनके कथ्य की एब्सर्डिटी को उभारने के लिए एब्सर्ड अप्रस्तुत विधान का सहारा लिया गया है। अतः मैंने उन्हें एब्सर्ड उपन्यास का नाम दिया है। आशा है, यह नाम स्वीकार्य होगा।
1-12-1971
नरेन्द्र कोहली
एक
भारत की राजधानी दिल्ली। इस दिल्ली का एक कॉलेज। कॉलेज काफी बिखरा-बिखरा
है। लड़के-लड़कियों के बहुत सारे दल इधर-इधर फैले हुए हैं। पतलूनें कसी
हुई और चपटी हैं। कमीज़ों के तीन-चार बटन खुले हुए हैं। भीतर से
गंदी-गंधाती बनियान नज़र आती है। आस्तीनें रुई की बत्ती के समान लपेटी हुई
हैं और सींकों जैसी बाँहें नज़र आ रही हैं। किसी के भी हाथ में कोई
कॉपी-किताब नहीं है। किसी-किसी ने दो-चार कागज़ और एक-आध किताब
मोड़-तरोड़कर अपनी जेबों में ठूँसी हुई है या हाथ में डायरी जैसी कोई चीज़
पकड़ रखी है।
लड़कियों ने चुस्त कमीज़ें और सलवारें पहन रखी हैं या फिर साड़ियाँ हैं, जो शरीर को बहुत आकर्षक रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। शकलों पर मनहूसियत है और सिरों पर ऊँचे-ऊँचे रूखे बाल। हाथों में बडे-बड़े पर्स हैं। उन पर्सों के भीतर की बात इस उपन्यास का लेखक नहीं जानता (या उनके विषय में लिखना नहीं चाहता)
ये अमीर और पढ़े़-लिखे, सभ्य-सुसंस्कृत पेरैंट्स के बच्चे हैं।
एक और दल भी है। इस दल में लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी। उनके कपड़े़ ढीले-ढाले और शैबी हैं। बालों में सरसों का तेल लगा हुआ है और काफी चपटी कंघी की हुई है। लड़कियों ने कसी हुई कुरूप चोटियाँ कर रखी हैं इन लोगों को हाथों में बहुत सारी पुस्तकें हैं। ये लोग कॉलेज की लायब्रेरी में बैठते हैं। सबसे डरते हैं। किसी से मन की बात नहीं करते। न ऊँचा बोलते हैं, न ऊँचा हँसते हैं। ये कॉलेज के बैकवर्ड लोग हैं। एकदम डल और भौंदू समझे जाते हैं। इनसे कोई बात करना भी पसन्द नहीं करता। ये लोग ऐसे मूर्ख हैं, केवल पढ़ने के लिए ही कॉलेज आते हैं।
ये गरीब और अनपढ़ माता-पिताओं के बच्चे हैं।
लड़कियों ने चुस्त कमीज़ें और सलवारें पहन रखी हैं या फिर साड़ियाँ हैं, जो शरीर को बहुत आकर्षक रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। शकलों पर मनहूसियत है और सिरों पर ऊँचे-ऊँचे रूखे बाल। हाथों में बडे-बड़े पर्स हैं। उन पर्सों के भीतर की बात इस उपन्यास का लेखक नहीं जानता (या उनके विषय में लिखना नहीं चाहता)
ये अमीर और पढ़े़-लिखे, सभ्य-सुसंस्कृत पेरैंट्स के बच्चे हैं।
एक और दल भी है। इस दल में लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी। उनके कपड़े़ ढीले-ढाले और शैबी हैं। बालों में सरसों का तेल लगा हुआ है और काफी चपटी कंघी की हुई है। लड़कियों ने कसी हुई कुरूप चोटियाँ कर रखी हैं इन लोगों को हाथों में बहुत सारी पुस्तकें हैं। ये लोग कॉलेज की लायब्रेरी में बैठते हैं। सबसे डरते हैं। किसी से मन की बात नहीं करते। न ऊँचा बोलते हैं, न ऊँचा हँसते हैं। ये कॉलेज के बैकवर्ड लोग हैं। एकदम डल और भौंदू समझे जाते हैं। इनसे कोई बात करना भी पसन्द नहीं करता। ये लोग ऐसे मूर्ख हैं, केवल पढ़ने के लिए ही कॉलेज आते हैं।
ये गरीब और अनपढ़ माता-पिताओं के बच्चे हैं।
दो
कॉलेज का एक दूसरा अंग उसकी बिल्डिंग है। बहुत लम्बी-चौड़ी बिल्डिंग है।
सारी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। ये पिछले विद्यार्थी-जागरण के चिह्न
हैं। इस कॉलेज के एक प्रोफेसर ने एक लड़के से कहा था और लड़के ने दूसरे
कॉलेज में पढ़ने वाले अपने एक दोस्त लड़के से कहा था,
‘‘माई डियर यार ! सारा स्टूडेंट-अनरेस्ट साला
तुम्हारे कॉलेज तक ही आकर रुक गया। हमारे हिस्से में कुछ नहीं पड़ा। नो,
पापे ! दिस इज़ नॉट गुड। कुछ अनरेस्ट कॉलेज में भी भेजो। वी विल मदद यू
!’’
दूसरे दिन, दूसरे कॉलेज के पाँच-सात लड़के और बाकी न पढ़ने वाले उन लड़कों के दोस्त लड़के—कुल मिलाकर चालीस-पचास लड़के—आए थे। उन्होंने पत्थर मार-मार कर खिलाड़ियों के सारे शीशे तोड़ दिए थे।
इस कॉलेज के उसी प्रोफेसर ने पुलिस को टेलीफोन किया था। उसी लड़के ने अपने क़लेज के लड़कों की ओर से पथराव का विरोध किया था। पुलिस आई थी। लड़के और उन लड़कों के दोस्त लड़के भागकर पुलिस के पास गए थे कि बाहर के लड़के आकर उनको पत्थर मार रहे हैं। पथराव रुक गया था। पुलिस चली गई थी—और इस कॉलेज में भी स्टूडेंट्स-जागृति और छात्र-अनरेस्ट आ गया था।
बिल्डिंग के कमरों के भीतर डेस्क और कुर्सियाँ एक—दूसरे पर पड़ी हैं, जिसका मतलब है कि थोड़ी देर पहले कुछ लड़के यहाँ बैठे हुए थे। जब वे आपस में मिलकर बैठते हैं तो धींगा-मस्ती ज़रूर करते हैं। एक-दूसरे को कुर्सियाँ और डेस्क फेंककर ज़रूर मारते हैं। न भी मारें तो फर्नीचर की उठा-पटक तो करते ही हैं। एक्टिव और स्मार्ट स्टूडेंट्स किसी कमरे को ठीक-ठाक नहीं रहने देते।
बिल्डिंग की दीवारों पर चाक पेंसिलों से और कहीं-कहीं कोयले से भी ढेर सारी चित्रकारी की गई है। इससे दीवारें अजन्ता और एलोरा की गुफाओं के समान चित्रमयी हो गई हैं। अधिकांश स्थानों पर परिवार-नियोजन से सम्बद्ध बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। सरकार का काम है, अतः जनता भी करती है। इस देश का युवक वर्ग अब अपना कर्तव्य समझने लगा है। युवक वर्ग जाग्रत है।
दूसरे दिन, दूसरे कॉलेज के पाँच-सात लड़के और बाकी न पढ़ने वाले उन लड़कों के दोस्त लड़के—कुल मिलाकर चालीस-पचास लड़के—आए थे। उन्होंने पत्थर मार-मार कर खिलाड़ियों के सारे शीशे तोड़ दिए थे।
इस कॉलेज के उसी प्रोफेसर ने पुलिस को टेलीफोन किया था। उसी लड़के ने अपने क़लेज के लड़कों की ओर से पथराव का विरोध किया था। पुलिस आई थी। लड़के और उन लड़कों के दोस्त लड़के भागकर पुलिस के पास गए थे कि बाहर के लड़के आकर उनको पत्थर मार रहे हैं। पथराव रुक गया था। पुलिस चली गई थी—और इस कॉलेज में भी स्टूडेंट्स-जागृति और छात्र-अनरेस्ट आ गया था।
बिल्डिंग के कमरों के भीतर डेस्क और कुर्सियाँ एक—दूसरे पर पड़ी हैं, जिसका मतलब है कि थोड़ी देर पहले कुछ लड़के यहाँ बैठे हुए थे। जब वे आपस में मिलकर बैठते हैं तो धींगा-मस्ती ज़रूर करते हैं। एक-दूसरे को कुर्सियाँ और डेस्क फेंककर ज़रूर मारते हैं। न भी मारें तो फर्नीचर की उठा-पटक तो करते ही हैं। एक्टिव और स्मार्ट स्टूडेंट्स किसी कमरे को ठीक-ठाक नहीं रहने देते।
बिल्डिंग की दीवारों पर चाक पेंसिलों से और कहीं-कहीं कोयले से भी ढेर सारी चित्रकारी की गई है। इससे दीवारें अजन्ता और एलोरा की गुफाओं के समान चित्रमयी हो गई हैं। अधिकांश स्थानों पर परिवार-नियोजन से सम्बद्ध बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। सरकार का काम है, अतः जनता भी करती है। इस देश का युवक वर्ग अब अपना कर्तव्य समझने लगा है। युवक वर्ग जाग्रत है।
तीन
उस बिल्डिंग के एक कोने में एक बड़ा-सा कमरा है। उसके दरवाज़ों पर बड़ी-सी
चिक लटक रही है और उस चिक से छनकर बहुत-सा शोर बाहर आ रहा है, जो बरामदों
में तैरता हुआ सारी बिल्डिंग में फैल जाता है।
चिक के भीतर शोर और भी ज़्यादा है। यहाँ कोई किसी को शोर मचाने से नहीं रोकता। यहाँ सच्चा स्वराज्य है। यहाँ वे लोग बसते हैं, जो केवल बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। स्टाफ-रूम है।
खिड़कियों के कपड़े वर्षों बाद धुलने गए हैं, अतः वर्षों बाद लौटेंगे।
इसलिए बाहर से कभी भी कोई चिड़िया या कौवा आकर खिड़की की सलाखों पर बैठ जाता है।
इस समय खिड़की की उन्हीं सलाखों में से एक पर बैठा हुआ एक कौवा बकवास कर रहा है।
और साथ-साथ स्टाफ-रूम में कुर्सियों पर बैठे-बैठे, सूट-बूट वाले लोग बकवास कर रहे हैं।
‘‘स्टूडेंट्स में इनडिसिप्लिन बहुत बढ़ रहा है।’’
‘‘देश में गरीबी बहुत बढ़ रही है।’’
‘‘गरीबी नहीं, महँगाई बढ़ रही है।’’
‘‘आपका दिमाग खराब है।’’
‘‘दिमाग खराब होगा आपका ! हम सही बात कर रहे हैं, क्योंकि डालडा खाते हैं।’’
‘‘एक्सेलसियर पर ‘यहूदी की बेटी’ लगी हुई है।’’
‘‘कल साला सब्ज़ीवाला सड़े हुए टिंडे दे गया।’’
‘‘कांग्रेस के राज में सड़े टिंडे नहीं बिकेंगे तो क्या बिकेगा !’’
‘‘महाशय ! पाँच सौ श्लोक याद हैं मुझे।’’
‘‘आपकी क्या बात है ! आप तो डिक्शनरी हैं, जनाब !’’
‘‘इन्हें उठवाकर पुस्तकालय में रखवा दो।’’
‘‘सुरैया ज़्यादा अच्छा गाती है लता से।’’
‘‘बकवास बन्द करो।’’
और कौवा बकवास बन्द करके उड़ गया !
चिक के भीतर शोर और भी ज़्यादा है। यहाँ कोई किसी को शोर मचाने से नहीं रोकता। यहाँ सच्चा स्वराज्य है। यहाँ वे लोग बसते हैं, जो केवल बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। स्टाफ-रूम है।
खिड़कियों के कपड़े वर्षों बाद धुलने गए हैं, अतः वर्षों बाद लौटेंगे।
इसलिए बाहर से कभी भी कोई चिड़िया या कौवा आकर खिड़की की सलाखों पर बैठ जाता है।
इस समय खिड़की की उन्हीं सलाखों में से एक पर बैठा हुआ एक कौवा बकवास कर रहा है।
और साथ-साथ स्टाफ-रूम में कुर्सियों पर बैठे-बैठे, सूट-बूट वाले लोग बकवास कर रहे हैं।
‘‘स्टूडेंट्स में इनडिसिप्लिन बहुत बढ़ रहा है।’’
‘‘देश में गरीबी बहुत बढ़ रही है।’’
‘‘गरीबी नहीं, महँगाई बढ़ रही है।’’
‘‘आपका दिमाग खराब है।’’
‘‘दिमाग खराब होगा आपका ! हम सही बात कर रहे हैं, क्योंकि डालडा खाते हैं।’’
‘‘एक्सेलसियर पर ‘यहूदी की बेटी’ लगी हुई है।’’
‘‘कल साला सब्ज़ीवाला सड़े हुए टिंडे दे गया।’’
‘‘कांग्रेस के राज में सड़े टिंडे नहीं बिकेंगे तो क्या बिकेगा !’’
‘‘महाशय ! पाँच सौ श्लोक याद हैं मुझे।’’
‘‘आपकी क्या बात है ! आप तो डिक्शनरी हैं, जनाब !’’
‘‘इन्हें उठवाकर पुस्तकालय में रखवा दो।’’
‘‘सुरैया ज़्यादा अच्छा गाती है लता से।’’
‘‘बकवास बन्द करो।’’
और कौवा बकवास बन्द करके उड़ गया !
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i